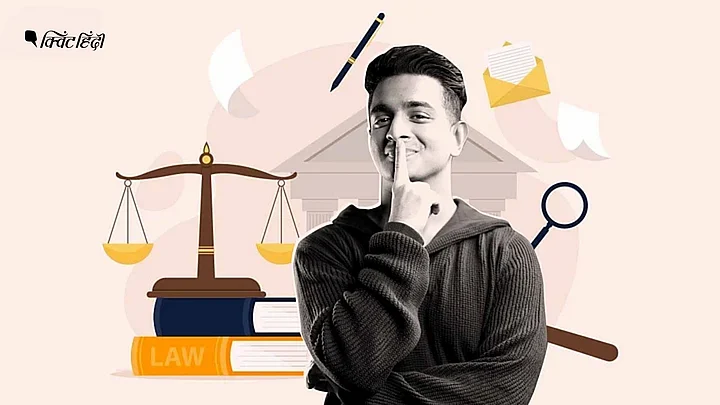कॉमेडी, अश्लीलता और असभ्यता अभिव्यक्ति की जमीन पर खड़े तीन स्तंभ हैं, जो आजादी और फ्री स्पीच में निहित हैं. आज के समय में कभी भी, कहीं भी, किसी के द्वारा भावनाएं आहत हो सकती हैं. और भारत जैसे देश में इसका जवाब अक्सर FIR के रूप में देखने को मिलता है.
कुछ हास्य कलाकारों (कॉमेडियन) द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक प्राइवेट शो करने से मीडिया घरानों में सनसनी फैल गई. आयोजकों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है. वहीं यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई FIR दर्ज हुए हैं.
शो में इलाहाबादिया द्वारा की गई टिप्पणी का कंटेस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ा- लेकिन उस जोक से जनता भड़क गई, जिसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल थे. ये वो अधिकारी हैं, जिन्होंने कभी इलाहाबादिया के साथ मंच साझा किया था और अब वे उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं.
महाराष्ट्र पुलिस अब उन लोगों की भी जांच कर रही है जिन्होंने शो में भाग लिया था और रिपोर्ट के अनुसार 40 से अधिक लोगों को तलब किया है. अब सवाल उठता है: अब जब लोग कॉमेडी और इसकी सीमाओं पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में कहां लाइन खींची जानी चाहिए?
जाहिर है कि लोगों की हर चीज को लेकर अपनी एक राय होती है, और उस राय के साथ आक्रोश भी देखने को मिलता है. ऐसे में, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह आक्रोश सिलेक्टिव है या फिर अडेप्टिव.
फ्री स्पीच के बीच नाजुक संतुलन
लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सार सबसे विवादास्पद अभिव्यक्तियों की भी रक्षा करने की क्षमता में निहित है, जब तक कि वे हिंसा या नफरत को न भड़काएं. इलाहाबादिया का जोक निस्संदेह कई लोगों के लिए भद्दा और असंवेदनशील था, लेकिन सिर्फ ठेस पहुंचना ही बोलने को अपराध मानने का पैमाना नहीं हो सकता. जैसे ही हम सीमाओं से आगे बढ़ने पर कॉमेडियन या कलाकारों को दंडित करना शुरू करते हैं, वैसे ही हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बुनियाद को खत्म करने का जोखिम भी उठा रहे होते हैं.
आयोजकों के खिलाफ आपराधिक आरोप समाधान नहीं हैं. वास्तव में इससे एक गलत मिसाल कायम होता है, जिससे सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल जाता है कि कौन सा हास्य स्वीकार्य है, जो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार पर हमला है.
जैसा कि वॉल्टेयर ने कहा था, "मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं मरते दम तक आपके बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा." यह सिद्धांत तब भी लागू होना चाहिए जब सामग्री अरुचिकर या उत्तेजक हो, जब तक कि वह उकसावे या नुकसान की सीमा को पार न कर जाए.
ऐसे समय में जब देश में कई अन्य अधिक गंभीर मुद्दे हैं - आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक असमानताएं और शासन की विफलताएं - कॉमेडियन को निशाना बनाना इन महत्वपूर्ण चिंताओं को छुपाने के लिए एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति की तरह दिखता है.
मार्टिन नीमोलर की कविता ‘फर्स्ट दे केम’ हमें याद दिलाती है कि जब हम सेंसरशिप के सामने चुप रहते हैं तो क्या होता है: “फिर वे मेरे लिए आए, और मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा.”
अगर हम आज सरकार को हास्य कलाकारों को चुप कराने की अनुमति देते हैं, तो अगला कौन होगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का मतलब हर बोले गए शब्द का समर्थन करना नहीं है, बल्कि बोलने के अधिकार की रक्षा करना है, तब भी जब हम उसको लेकर असहज हों.
कानूनी परिदृश्य
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 294 अश्लील सामग्री की बिक्री से संबंधित है. पिछले कानून की तुलना में इस प्रावधान की भाषा में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें “इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी सामग्री का प्रदर्शन” शामिल है. सवाल यह है कि क्या इस तरह के मामले नए प्रावधान के तहत आएंगे, यह बात फैसला ट्रायल कोर्ट को तय करना है.
इससे पहले, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 292 (2) के तहत किसी भी अश्लील सामग्री की बिक्री, किराए पर देने, प्रसारित करने और वितरण पर दंड लगाया जाता था. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 भी ऐसे टेलीविजन प्रसारणों को नियंत्रित करता है जो सार्वजनिक आक्रोश को भड़का सकते हैं.
'हिक्लिन टेस्ट' के जरिए पहले यह निर्धारित किया गया कि अश्लीलता क्या होती है. साथ ही उन चीजों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया जो संवेदनशील दर्शकों, विशेष रूप से बच्चों को "बिगाड़ और भ्रष्ट" कर सकती है. बता दें कि रेजिना बनाम हिक्लिन (1868) मामले से हिक्लिन टेस्ट की उत्पत्ति हुई थी.
हालांकि, रंजीत उदेशी बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अश्लीलता की अवधारणा समय के साथ विकसित होती है और जो चीज एक समय में "अश्लील" रही होगी, वह बाद में अश्लील नहीं रहेगी. जजमेंट में अश्लीलता की बदलती धारणा के कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया है और अंततः कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:
"दुनिया अब विभिन्न प्रकार के साहित्य से प्रभावित होकर पहले की तुलना में बहुत अधिक सहन करने में सक्षम है. रवैया अभी भी तय नहीं हुआ है."
बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधात्मक हिकलिन परीक्षण से दूरी बना ली और कहा कि सामग्री का मूल्यांकन "एक उचित, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी व्यक्ति के मानकों से किया जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के नजरिए से या उन लोगों के नजरिए से जो हर प्रतिकूल दृष्टिकोण में खतरा महसूस करते हैं."
अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल सरकार (2014) मामला, सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकाशन से संबंधित मामले पर विचार कर रहा था जिसमें एक पत्रिका में नग्न जोड़े की तस्वीर प्रकाशित की गई थी. इस मामले में, हिक्लिन टेस्ट से मिलर टेस्ट तक एक प्रतिमान बदलाव हुआ, जिसका प्रयोग अमेरिका में किया गया था, और कहा गया कि अश्लीलता का मूल्यांकन पूरे कार्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि अलग-अलग दृश्यों या छवियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
पुराने मामले: जब कॉमेडी अपराध बन गई
जनवरी 2016 में, कॉमेडियन-अभिनेता कीकू शारदा को एक टेलीविजन शो में बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह का किरदार निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था. शारदा पर “धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने” का आरोप लगाया गया था और उन्हें एक दिन जेल में बिताना पड़ा था.
कुछ महीने बाद ही मई में, ऑल इंडिया बकचोद (एआईबी) के सह-संस्थापक तन्मय भट्ट पर एक वीडियो के लिए आपराधिक आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और गायिका लता मंगेशकर की नकल की थी. एफआईआर के अनुसार, उन्होंने बड़े पैमाने पर "सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई".
जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कॉमेडी कब अपराध बन जाती है, तो हमें कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के मामले को नहीं भूलना चाहिए. जनवरी 2021 में फारुकी को कॉमेडियन नलिन यादव और अन्य के साथ मध्य प्रदेश में हिंदू देवताओं को लेकर कथित तौर पर जोक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई जोक किया भी था या नहीं. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले उन्होंने लगभग पांच हफ्ते जेल में बिताए.
कुछ महीने बाद, भारत के सबसे मशहूर कॉमेडियन वीर दास को उनके शो "आई कम फ्रॉम टू इंडियाज" के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने भारत में सामाजिक विरोधाभासों और पाखंड को उजागर किया था. शो के बाद, कई लोगों ने दास पर "भारत को बदनाम करने" का आरोप लगाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई.
भारत में कॉमेडी का भविष्य
ये घटनाएं एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करती हैं, जहां सार्वजनिक भावनाएं अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को दरकिनार कर देती हैं, और चुटकुलों को अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीरता से ले लिया जाता है.
विडंबना यह है कि समाज बड़े पैमाने पर गंभीर अन्यायों से अछूता रहता है - दोषी बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है, विचाराधीन कैदियों को जेल में बंद किया जाता है, या राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है- जबकि आक्रोश केवल हास्य कलाकारों तक सीमित रहता है.
यह चयनात्मक संवेदनशीलता एक समाज के रूप में हमारी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है. हम व्यवस्थागत विफलताओं और जघन्य अपराधों पर आंखें क्यों मूंद लेते हैं, लेकिन हास्य को अपराध घोषित करने में जल्दबाजी क्यों करते हैं, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो?
यह एक विकृत नैतिकता का प्रतिबिम्ब है, जहां लोग समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों को छोड़कर अपना आक्रोश हास्य कलाकारों पर निकाल रहे हैं.
जिस शो की वजह से इलाहाबादिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई, उसी शो में विकलांगता का मजाक उड़ाने और बॉडी शेमिंग के मामले भी सामने आए, फिर भी इन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया. आक्रोश चुनिंदा क्यों है? क्यों गंभीर, व्यवस्थागत मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि कॉमेडियन को उनके शब्दों के लिए अपराध का सामना करना पड़ता है?
ऐतिहासिक रूप से, राजद्रोह कानूनों का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता था. हालांकि राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन नए BNS प्रावधान और भी अधिक कठोर हैं.
भारत में कॉमेडी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी सीमाओं का अंतर-संबंध एक विवादास्पद और उभरता हुआ मुद्दा बन गया है. हास्य कलाकार जब भी नए मुद्दों पर बात करने और मनोरंजन के लिए सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हैं, हास्य और अपमान के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जाती है.
कॉमेडी की कोई सीमा नहीं होती- जब यह अपनी सीमा लांघ जाती है, तो हम इसे ‘डार्क कॉमेडी’ कहते हैं. लेकिन मजाक को मजाक ही समझना चाहिए.
एस तमिलसेल्वन बनाम तमिलनाडु सरकार केस के फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल ने जो बात लिखी थी, उसे याद करना सही है,
"जो पहले स्वीकार्य नहीं था, वह बाद में स्वीकार्य हो गया. लेडी चैटर्लीज लवर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. पढ़ने का विकल्प हमेशा पाठक के पास होता है. अगर आपको कोई किताब पसंद नहीं आती है, तो उसे फेंक दीजिए. किताब पढ़ना कोई मजबूरी नहीं है. साहित्यिक रुचियां अलग-अलग हो सकती हैं- जो किसी के लिए सही और स्वीकार्य है, वह दूसरों के लिए सही और स्वीकार्य नहीं हो सकता. फिर भी, लिखने का अधिकार निर्बाध है. अगर सामग्री संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देने या उसके खिलाफ जाने, नस्लीय मुद्दा उठाने, जातियों को बदनाम करने, ईशनिंदा वाले संवाद रखने, अस्वीकार्य यौन सामग्री रखने या हमारे देश के अस्तित्व के विरुद्ध युद्ध शुरू करने का प्रयास करती है, तो सरकार निस्संदेह हस्तक्षेप करेगी."
(अरीब उद्दीन अहमद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं. वह विभिन्न कानूनी घटनाक्रमों पर लिखते हैं. यह एक ओपिनियन पीस है और ऊपर व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट न तो इसका समर्थन करता है और न ही इसके लिए जिम्मेदार है.)