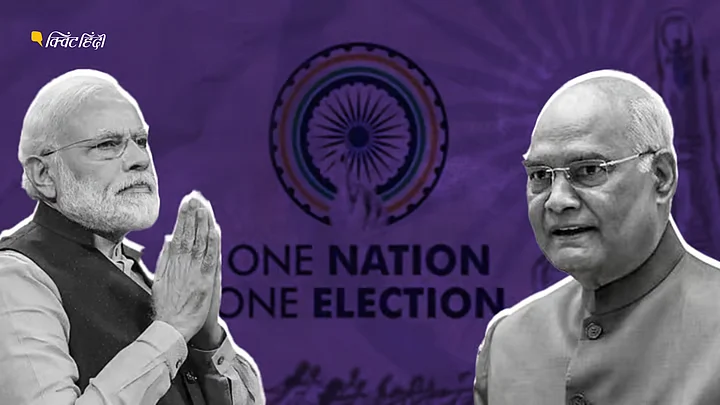एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election) एक ऐसा विचार है जो सुनने में तो अच्छा लगता है - लेकिन यह भारत के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा. इसके कथित लाभ झूठे हैं, और हमारा इतिहास बताता है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री लोगों के लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक गणित के आधार पर एक साथ या अलग-अलग चुनाव कराने के बारे में सोचते हैं.
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत की राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव करने के लिए कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. एक राष्ट्र एक चुनाव का पहली बार प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में दिया था और पिछले साल उन्होंने इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया था.
12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयकों को मंजूरी दी गई.
इतिहास पर एक नजर
1951 से 1962 तक, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले तीन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित करवाये, क्योंकि वह और उनकी कांग्रेस पार्टी देश भर में बेहद लोकप्रिय थी. पार्टी ने लगभग सभी राज्यों में बहुमत हासिल किया और नेहरू ने अपने मुख्यमंत्रियों को खुद चुना और पूरे देश को नई दिल्ली से चलाया.
भारत के संविधान के प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने लिखा है, "केन्द्र और अधिकांश राज्य सरकारों में पार्टी और सरकार जुड़वां भाई-बहन थे, जो सिर, कूल्हे और पैर से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे."
लेकिन जब 1967 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत घटकर 25 रह गया और पार्टी आठ राज्यों में हार गयी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को अलग करने का फैसला लिया. उन्होंने गरीबी हटाओ अभियान के तहत एक प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किया, एक साल पहले ही लोकसभा भंग कर दी और 1971 में चुनाव घोषित कर दिए. उनकी कांग्रेस (आर) ने 520 में से 350 सीटें जीतीं, जिससे उन्हें दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ.
हालांकि, श्रीमती गांधी ने तमिलनाडु को अलग नहीं किया. उस राज्य में, मुख्यमंत्री करुणानिधि ने भी विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया और श्रीमती गांधी के साथ गठबंधन कर लिया ताकि उनके एक दुश्मन के कामराज को हराया जा सके.
प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार एक साथ या अलग-अलग चुनाव कराने की यह परंपरा देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है. उदाहरण के लिए, भारत की संघीय व्यवस्था पर इसके घातक प्रभावों के बारे में सोचें. हमारे देश के आकार और विविधता को देखते हुए, यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि राज्य के मुद्दे, नेता और पार्टियां प्रमुखता से उभरें. राज्य के चुनावों का महत्व कम करना- जो कि राष्ट्रीय दलों, नेताओं और मुद्दों के साथ मिलकर होना तय है- इससे केवल स्थानीय जवाबदेही को ही नुकसान पहुंचेगा.
इस बात पर भी गौर करें कि एक राष्ट्र एक चुनाव इस बुनियादी संसदीय सिद्धांत का कितना मजाक उड़ाता है कि सरकारों को किसी भी समय जवाबदेह ठहराया जा सकता है और गिराया जा सकता है. यह मुख्य लाभ है जिसे हमारे संस्थापकों, विशेष रूप से बीआर अंबेडकर ने संसदीय प्रणाली के अपने चयन के लिए उद्धृत किया था.
ऑर्डर पर तैयार रिपोर्ट?
अगर कोई सरकार गिरती है और एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत नया चुनाव होता है, तो नई सरकार का कार्यकाल छोटा करना होगा और यही कोविंद समिति की सिफारिश है. यह न केवल प्रचार करने वालों और जीतने वालों के प्रति अनुचित है, बल्कि अलोकतांत्रिक भी है. लोग अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार चुनते हैं, लेकिन कुछ महीनों के लिए चुनी गई सरकार न तो वादे पूरे कर सकती है और न ही उसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है.
मोदी के विरोधियों ने आरोप लगाया है कि कोविंद समिति की रिपोर्ट मनमाने ढंग से तैयार की गई थी. अगर आप रिपोर्ट का मूल्यांकन इसके मुख्य तर्क से करें तो यह आरोप उचित है, कि कई चुनाव कराने से "सरकार, व्यवसाय, श्रमिकों, न्यायालयों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर नागरिक समाज पर भारी बोझ पड़ता है."
भारत एक ओर तो विश्व का सबसे बड़ा समृद्ध लोकतंत्र होने का दावा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर चुनाव कराने को बोझ नहीं मान सकता. क्या हमारे लोकतंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण और लोगों द्वारा अपने नेता चुनने से ज्यादा बुनियादी कोई चीज है?
इसके अलावा, इस बोझ को कम करने के लिए समिति की सिफारिशें वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं हैं. इसमें चुनावों की संख्या को मौजूदा तीन (लोकसभा, राज्य और पंचायत) से घटाकर दो (लोकसभा और राज्य और 100 दिन बाद पंचायत) करने का सुझाव दिया गया है. अगर आप लोकसभा और राज्य चुनावों को मिला दें तो भी उम्मीदवार, कार्यकर्ता, पार्टियां और सिविल सोसायटी प्रत्येक चुनाव के लिए अलग-अलग प्रचार करेंगे.
सरकारों और व्यवसायों पर बोझ में भी ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यह एक मिथक है कि चुनावों के दौरान नैतिक आचार संहिता सभी सरकारी कामों को रोक देती है. यह संहिता केवल सरकारों को नई योजनाएं शुरू करने या कर्मचारियों के स्थानांतरण शुरू करने से रोकती है.
इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी और उनकी पार्टी के सहयोगी बहुत अधिक चुनावों के बोझ से दबे हुए हैं. लेकिन केंद्र या प्रधानमंत्री को हर राज्य के चुनाव में शामिल होने का क्या काम है? इससे स्थानीय जवाबदेही को ही नुकसान पहुंचता है. अगर भारत राज्य सरकारों को ज्यादा स्वतंत्र होने दे- अलग-अलग निर्वाचित, स्थानीय मुद्दों पर आधारित, स्थानीय नेताओं द्वारा संचालित, उनके वित्त पर ज्यादा नियंत्रण- तो जमीनी स्तर पर हमारा शासन बेहतर होगा. और एक राज्य के चुनाव से दूसरे राज्यों या केंद्र पर बोझ नहीं पड़ेगा.
कोविंद समिति का यह भी तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और चुनावी खर्च में कमी आएगी. यह मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि एक साथ चुनाव कराने से “निश्चितता” आएगी. लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बारे में कोई कितना निश्चित हो सकता है कि केंद्र या राज्य में संसदीय सरकार कब गिर जाएगी? समिति भारत में सरकारों को गिराने के लिए कुख्यात राजनीति और खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाती है.
जहां तक चुनावी खर्च का सवाल है, समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारें वर्तमान में राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने में लगभग 4,500 करोड़ रुपये खर्च करती हैं. यह प्रत्येक पात्र मतदाता के लिए 50 रुपये से भी कम है और इसे हमारे लोकतंत्र में एक सार्थक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए. वास्तव में यह फिजूलखर्ची वाला पैसा पार्टियों और प्रचार अभियानों पर खर्च किया जाता है; समिति का अनुमान है कि यह 4-7 लाख करोड़ रुपये है. चूंकि यह काफी हद तक काला धन है, इसलिए यह सोचना भोलापन होगा कि इसे एक साथ होने वाले चुनावों में मतदाताओं को लुभाने पर खर्च नहीं किया जाएगा.
कोई भी इसके लिए शोर नहीं मचा रहा है
एक साथ चुनाव कराने के बारे में आम गलतफहमी है कि ये राष्ट्रपति शासन प्रणाली के समान हैं. सच्चाई इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती.
समिति ने केवल छह देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, आदि) की चुनाव प्रणालियों का अध्ययन किया, लेकिन ब्रिटेन या अमेरिका का अध्ययन नहीं किया. उदाहरण के लिए, अमेरिका में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय विधानसभाएं न केवल अलग-अलग चुनी जाती हैं, बल्कि उनका कार्यकाल भी अलग-अलग होता है. उनके प्रतिनिधि सदन (लोकसभा) का चुनाव हर दो साल में होता है, लेकिन राष्ट्रपति चार और सीनेटर छह साल के लिए काम करते हैं.
सच तो यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोगों की सेवा के लिए नहीं बनाया गया है. कोई भी इसके लिए शोर नहीं मचा रहा है और न ही हम चुनाव की थकान से पीड़ित हैं, जैसा कि मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी के स्तर से पता चलता है. हमारे भारतीय लोकतंत्र को अधिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, न कि अधिक केंद्रीकरण की.
(लेखक दिव्य हिमाचल समूह के संस्थापक और सीईओ हैं और ‘भारत को राष्ट्रपति प्रणाली की आवश्यकता क्यों है’ किताब के लेखक हैं. उनसे X पर @BhanuDhamija पर संपर्क किया जा सकता है. यह एक निजी ब्लॉग है और ऊपर व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट न तो इसका समर्थन करता है और न ही इसके लिए जिम्मेदार है.)