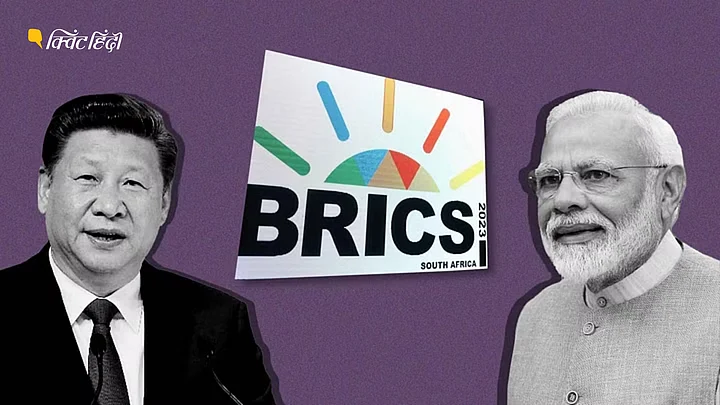15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) 22-24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने हिस्सा लिया. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) भी इसमें शामिल हुए. शिखर सम्मेलन के कामकाज से ज्यादा सबका ध्यान इन दोनों नेताओं के बीच संभावित बैठक पर केंद्रित था.
इसकी वजह पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत-चीन के बीच जारी तनाव है. 2020 में LAC पर चीनी अतिक्रमण के कारण उभरे कुछ मुद्दों को हल कर लिया गया है, लेकिन चीनी अतिक्रमण से पहले 2020 में जो स्थिति थी, उसे बहाल नहीं किया गया है.
यह स्थिति कोर कमांडरों के स्तर पर 19 दौर की सैन्य वार्ता और मंत्री स्तर समेत राजनीतिक और कूटनीतिक विचार-विमर्श के बावजूद है.
दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बयानों में अंतर
मोदी और शी जिनपिंग के बीच 23 अगस्त को जोहान्सबर्ग में बातचीत हुई थी. आधिकारिक टिप्पणी में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, जिसे उन्होंने "बातचीत" बताया था, पहल PM मोदी की ओर से की गई थी. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने चीन के इस दावे पर 'ऑन-द-रिकॉर्ड' टिप्पणी नहीं की है. निश्चित रूप से, चीनी प्रवक्ता के लिए भी इस प्वाइंट का जिक्र करना जरूरी नहीं था.
मोदी-शी जिनपिंग की बातचीत पर भारत और चीन के तरफ से जो ब्यौरे दिए जा रहे हैं वो एक नहीं हैं. दोनों ने LAC स्थिति पर मौजूदा राष्ट्रीय रुख को दोहराया.
इसी प्रकार, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जोहान्सबर्ग में मीडिया से कहा, "चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में, प्रधानमंत्री ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं को उठाया है”.
यह भारत की स्थिति का हिस्सा है कि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति तब तक बहाल नहीं की जा सकती जब तक कि 2020 में चीन के एक्शन से खड़े हुए सीमा से जुड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते.
सीमा-विवाद के मुद्दे पर क्या?
चीनी प्रवक्ता ने बताया कि शी जिनपिंग ने मोदी से कहा था कि "भारत-चीन संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के साझा हितों को पूरा करता है".
जहां तक सीमा मुद्दों का सवाल है, शी ने कहा, "दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों को ध्यान में रखना चाहिए और सीमा मुद्दे को ठीक से संभालना चाहिए ताकि संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति की रक्षा की जा सके". चीन का यह पुराना स्टैंडर्ड रुख रहा है जिसे उसने इस बार भी दोहरा दिया.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, विदेश सचिव क्वात्रा ने ये कहा है कि ‘दोनों देश के नेता अपने अधिकारियों को अभियान से सैनिकों को हटाने और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देंगे", लेकिन चीन की तरफ के बयान में इस प्वाइंट पर चुप्पी है.
इस तरह के बयान और पुराने रुख को ही दोनों देश के सबसे शिखर नेताओं की बात में दोहराया जाना इस बात का इशारा नहीं करता है कि सीमा संबंधी समस्याएं जल्द निपटने वाली हैं.
और अब शिखर सम्मेलन पर, क्योंकि इससे शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं का भी पता चला है. ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई उसे देखने पर इस परिप्रेक्ष्य को ठीक से समझा जा सकता है.
चीन-अमेरिका की रेस का BRICS पर असर
2001 में जब न्यूयॉर्क के एक निवेश बैंकर के BRICS समूह बनाने के और 2009 के पहले BRICS शिखर सम्मेलन और अभी दक्षिण अफ्रीका में संपन्न 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तक अंतर्राष्ट्रीय हालात काफी बदल चुके हैं.
2001 की तो बात ही छोड़ ही दीजिए, 2009 में चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता, जो मौजूदा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और जियो-इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फैक्टर है, वो कहीं थी ही नहीं. अब, सभी देश और समूह इससे प्रभावित हैं. ब्रिक्स कोई अपवाद नहीं है.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जोहान्सबर्ग घोषणा में चीन ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल हुआ. घोषणापत्र में एक समान ग्लोबल ऑर्डर की बात की गई है जो सभी देशों के हितों की रक्षा करे.
ये सब चिकनीचुपड़ी बातें हैं, जो दिखने में काफी अच्छी लगती है. चीन यह दिखाना चाह सकता है कि वह एक इमर्जिंग कंट्री यानि उभरता हुआ देश है जिसके हित दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलते जुलते हैं. हालांकि, इस तरह के मुखौटे से अभी की अतंरराष्ट्रीय परिस्थिति की समझ नहीं मिलती है. साथ ही यह चीनी आक्रामकता को भी साफ नहीं करता.
BRICS के विस्तार में चीन का दबदबा
तथ्य यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन ने डेंग जियाओपिंग की सलाह से किनारा कर लिया है. डेंग ने सैन्य और रणनीतिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों मे बिना ज्यादा असरदार दिखे विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी लेकिन अब शी की अगुवाई वाले चीन में इस नीति को छोड़ दिया गया है.
अब कई वर्षों से, शी जिनपिंग ने लगातार इस दृढ़ संकल्प को दिखाया है कि यदि अमेरिका को दुनिया की सबसे पावरफुल देश वाली स्थिति से हटाया नहीं जा सके तो कम से कम चीन को बराबरी की पोजिशन जरूर मिलनी चाहिए. इसके लिए उसे उन समूहों में अपना रास्ता बनाने की आवश्यकता है जिनका वह सदस्य है.
यह कोई रहस्य नहीं है कि चीन ब्रिक्स का विस्तार चाहता था और उसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया.
छह नए सदस्यों - अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने पर निस्संदेह अन्य देश सहमत थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए सदस्यों के शामिल होने का स्वागत किया.
उन्होंने कहा, ''...भारत ने हमेशा ब्रिक्स सदस्यता के विस्तार का पूरा समर्थन किया है. भारत का हमेशा से मानना रहा है कि नए सदस्यों के शामिल होने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत होगा और हमारे सामूहिक प्रयासों को नई गति मिलेगी. यह कदम दुनिया के कई देशों का बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करेगा. मुझे खुशी है कि हमारी टीमें विस्तार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर एक समझौते पर पहुंची हैं."
भारत का रूख
मोदी ने आगे कहा कि ब्रिक्स का "विस्तार" और "आधुनिकीकरण" वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार के लिए संकेत है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी में बनाई गई ग्लोबल संस्थाएं आज की हकीकत को नहीं दिखाती हैं.
यह दशकों से भारत का रुख रहा है. मोदी उनमें सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा करके सही ही कर रहे थे. मुद्दा यह है कि क्या ब्रिक्स का विस्तार करने का यह कदम इसमें मदद करेगा. इस प्रश्न का यथार्थवादी विश्लेषण आवश्यक है.
ब्रिक्स के मूल रूप से चार सदस्य थे - रूस, चीन, ब्राजील और भारत. दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हुआ. मूल चार में ब्राजील और भारत, जापान और जर्मनी के साथ (जी4) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहे थे. रूस और चीन ने चाहे इस बारे में कहा जो कुछ भी हो लेकिन सुधार पर कुछ किया नहीं. भारत-रूस और भारत-चीन संयुक्त वक्तव्य में सुधार को लेकर भले ही कुछ भी कहा जाता रहा हो लेकिन मौजूदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना को बदलने के लिए उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली.
वह स्थिति नहीं बदली है. नए सदस्यों में से, अर्जेंटीना और मिस्र यूएनएससी विस्तार के मुद्दे पर जी4 का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं, जबकि अन्य चार इस मुद्दे पर भारत और ब्राजील के पक्ष में खुद को खड़ा नहीं रखते हैं.
दक्षिण अफ्रीका खुद को UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए स्वाभाविक अफ्रीकी उम्मीदवार मानता है, लेकिन अन्य अफ्रीकी देशों के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता है. संक्षेप में, यह संभावना नहीं है कि ब्रिक्स विस्तार से UNSC सुधार को बढ़ावा मिलेगा.
क्या आर्थिक ताकत के तौर पर अमेरिका का जवाब चीन हो सकता है?
इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन अभी हैं जैसे IMF, वर्ल्ड वैंक .. ये सबके सब ब्रेटॉन वुड इंस्टीट्यूशन हैं और ये अमेरिका और इसके सहयोगी पश्चिमी देशों के असर में रहते हैं.
2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट के बाद, जो अपने वित्तीय क्षेत्र के अमेरिकी कुप्रबंधन के कारण हुआ था, इन संस्थानों के भीतर अन्य देशों के लिए अधिक प्रभावी आवाज की मांग उठी थी. तब बैकफुट पर आए अमेरिका ने संकेत दिया कि वह अपनी पकड़ ढीली करेगा. लेकिन अभी तक इस दिशा में पर्याप्त एक्शन नहीं हुए.
इस बीच, चीनी अर्थव्यवस्था काफी बढ़ी है और ब्रिक्स के अन्य सदस्यों, खासकर भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी बढ़ी है - हालांकि चीन की तुलना या फिर चीन के बराबर बिल्कुल नहीं.
इसलिए, चीन एक विस्तारित ब्रिक्स चाहता है ताकि ब्रेटन वुड्स संस्थानों पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए अमेरिका पर दबाव जारी रखा जा सके, जबकि वह वैश्विक दक्षिण के देशों की वित्तीय सहायता के लिए ब्रिक्स संस्थानों को मजबूत करने की कोशिश करेगा.
चीन आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की पकड़ को कमजोर करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य और वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए अन्य व्यवस्थाओं की ओर कदम बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएगा. इन सब में चीन के साथ भारत के हितों का संयोग तो है लेकिन एक हद तक ही.
बहुपक्षवाद पर बंटा विश्व
'बहुध्रुवीय दुनिया' को लेकर भारत की राय बहुत पुरानी है. यह आजादी के शुरुआती साल से ही इस पक्ष में है, भले ही उस समय इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था. अनिवार्य रूप से, इसका मतलब यह है कि दुनिया पर एक या दो शक्तियों का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए जो पूरी दुनिया या वर्ल्ड ऑर्डर को अपने मुताबिक हांके.
यह मांग है कि अंतरराष्ट्रीय शासन के लिए नियम बनाने में भारत सहित कई महत्वपूर्ण देशों की भागीदारी होनी चाहिए और इन नियमों में ग्लोबल साउथ के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
जोहान्सबर्ग घोषणापत्र ने ब्रिक्स की "समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता" को दोहराया. शी जिनपिंग वाले चीन के आचरण से साफ तौर पर पता चलता है कि उसे बहुपक्षवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि अगर उसके हित दांव पर हैं तो वह अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के फैसलों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाता है.
घोषणापत्र में "एकतरफा जबरदस्ती उपायों" के लिए ब्रिक्स के विरोध का उल्लेख किया गया - रूस के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रतिबंधों का एक स्पष्ट संदर्भ दिया गया - लेकिन इस तरह की चीजें बहुत कम हैं और बड़ा ग्रुप बनने या विस्तारित BRICS भी इसे रोकने में शायद ही कुछ कर सके.
जोहान्सबर्ग घोषणापत्र ने BRICS के तीन स्तंभों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई. राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों का आपसी संपर्क. ये उद्देश्य ठीक हैं लेकिन यह पहले से ही एक अलग समूह है और इसका विस्तार इसमें और इजाफा करेगा. वह भी तेजी से चीन के प्रभाव में आ जाएगा. भारत की चुनौती उस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की होगी जो देश की प्रगति के बावजूद आसान नहीं होगी.
(लेखक विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव (पश्चिम) हैं. उनका ट्विटर हैंडिल @VivekKatju है. यह एक ओपिनियन पीस है, और ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट न तो उनका समर्थन करता है और न ही उनके लिए ज़िम्मेदार है.)