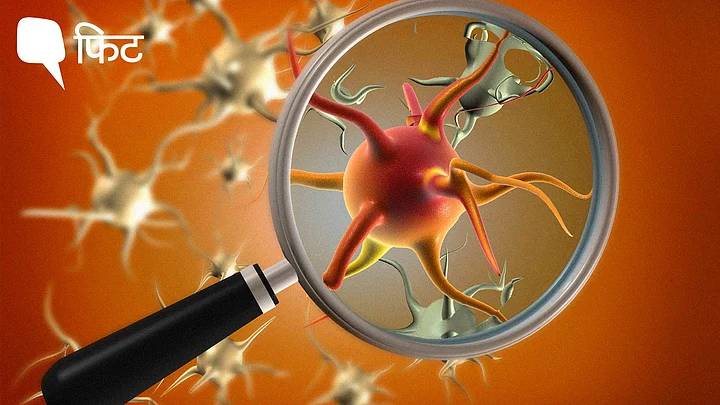World Health Day 2024: इंफेक्शियस डिजीज (Infectious Diseases) आज भी भारत में पब्लिक हेल्थ के मामले में बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. देश में आज भी बड़ी संख्या में लोग हर साल संक्रामक रोगों की वजह से मौत के शिकार बनते हैं, जबकि एक दूसरा पहलू यह भी है कि गैर-संक्रामक रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
भारत में ऐसे रोग चिंता का प्रमुख विषय बने हुए हैं, जिनसे बचा जा सकता है.
भारत में इंफेक्शियस डिजीज किस हद तक सेहत के लिए खतरा हैं? जानलेवा इंफेक्शियस डिजीज कौन-कौन से हैं? कैसे बचें? हमने एक्सपर्ट्स से पूछे ये सवाल और जानें इनके जवाब. आइए पढ़ते हैं.
भारत में इंफेक्शियस डिजीज किस हद तक सेहत के लिए खतरा हैं?
भारत में इंफेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग का प्रसार काफी अधिक है. स्वच्छता का अभाव, स्वच्छ पानी तक पहुंच और पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने की वजह से ऐसे रोगों के पनपने के लिए पूरा माहौल तैयार होता है. उस पर अपर्याप्त हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन रोगों के प्रसार में सहायक होता है.
"दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इन रोगों की वजह से इंफेक्शियस डिजीज की चपेट में आई हुई आधी से ज्यादा आबादी 50 साल की उम्र से पहले ही मौत की शिकार बन जाती है. बेशक, इन रोगों की वजह से होने वाली मौतों में कमी आयी है, लेकिन फिर भी ये रोग काफी नुकसान पहुंचाते हैं."डॉ. राजीव गुप्ता, डायरेक्टर – इंटरनल मेडिसिन, सी के बिड़ला अस्पताल®, दिल्ली
डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा डेटा से अपनी बात समझाते हुए कहती हैं,
"संक्रामक रोगों के बढ़ते बोझ का असेसमेंट करने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड की स्टडी के मुताबिक, संक्रामक रोगों से मरने वाले की संख्या 2021 में 86% बढ़कर 12,598 जा पहुंची है जबकि 2019 में यह आंकड़ा 6,767 रहा था."डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा, कंसलटेंट-इंफेक्शियस डिजीज, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
भारत के 7 प्रमुख इंफेक्शियस डिजीज कौन-कौन से हैं?
डॉ. राजीव गुप्ता बताते हैं कि भारत में संक्रामक रोगों का बोझा काफी ज्यादा है और 50 साल से कम उम्र वाले मरीजों में करीब 50% मौतों का कारण भी ये रोग हैं.
यहां 6 प्रमुख संक्रामक रोगों और उनसे संबंधित मौतों के आंकड़े (जहां उपलब्ध हैं) दिए जा रहे हैंः
1. ट्यूबरक्लॉसिस (TB): पिछले साल ट्यूबरक्लॉसिस (तपेदिक/टीबी) के करीब 2.55 मिलियन मामले दर्ज हुए थे. यह राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.
"इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 में TB के जोखिमों में कुपोषण या कम पोषण, एचआईवी और डायबिटीज का जिक्र किया गया है."डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा, कंसलटेंट-इंफेक्शियस डिजीज, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में इस वायरस से ग्रस्त 95% लोगों का इलाज किया गया है, जो कि देश में 2023 के एलिमिनेशन लक्ष्य की प्राप्ति का सूचक है. इसके अलावा भी अन्य कई स्तरों पर प्रयास जारी हैं और वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भी फिलहाल ट्रायल्स चल रहे हैं, उम्मीद है कि हम आने वाले समय में इस पुराने मर्ज पर बेहतर ढंग से काबू पा सकेंगे.
डॉ. राजीव गुप्ता मरीजों में इलाज अधूरा छोड़ने की बात बताते हैं.
"एक और बड़ी चिंता मरीजों द्वारा इलाज अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जैसे MDR-TB औरXDR-TB सामने आए हैं."डॉ. राजीव गुप्ता, डायरेक्टर – इंटरनल मेडिसिन, सी के बिड़ला अस्पताल®, दिल्ली
2. टाइफायड: यह सैलमोनेला बैक्टीरिया की वजह से होने वाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन है, जो प्रदूषित पानी और गदंगी की वजह से फैलता है.
"हालांकि वैक्सीन से कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन बेहतर हाइजीन और सैनिटेशन रोग को कंट्रोल करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं."डॉ. राजीव गुप्ता, डायरेक्टर– इंटरनल मेडिसिन, सी के बिड़ला अस्पताल®, दिल्ली
पिछले साल बारिश के मौसम में टाइफायड के मामलों में लगभग 30% बढ़ोतरी हुई थी. इसका बड़ा कारण ड्रग-रेजिस्टेंट टाइफायड का प्रकोप था. भारत में यह रोग हर साल लगभग 45 लाख लोगों को शिकार बनाता है और इसकी वजह से लगभग 9000 मौतें होती हैं. शहरी भारत में भी टाइफायड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.
"हम सलाह देते हैं कि खासतौर से बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को जटिलताओं से बचाने और रोग को दोबारा पनपने नहीं देने के लिए, टाइफायड वैक्सीन यानी टीसीवी (कंज्यूगेटेड वैक्सीन) और नॉन कंज्यूगेटेड पोलीसैकराइड वैक्सीन (ViCPS) लेनी चाहिए."डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा, कंसलटेंट-इंफेक्शियस डिजीज, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
समय पर वैक्सीन लेने, ओरल हाइजीन अच्छी रखने, पानी और खानपान सेहतमंद रखने से इस रोग से बचाव किया जा सकता है.
3. डेंगू: देश में पिछले साल नवंबर के मध्य तक करीब 2 लाख डेंगू के मामले सामने आए थे. ये मामले ज्यदातर दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में दर्ज किए गए हैं. देखा गया है कि डेंगू का वायरस गर्म तापमान में पनपता है. तापमान में बढ़ोतरी होने पर एडिस मच्छर को पनपने और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है. डेंगू के कई लक्षण हो सकते हैं, जिसमें बुखार से लेकर ब्लीडिंग और कई बार गंभीर शॉक भी हो सकता है. इसके अलावा,
बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, वैक्सीन लें और साफ-सफाई पर पूरा ध्यान दें.
"इस रोग से जुड़ी कई गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं, ऐसे में मच्छर से बचाव के उपायों पर खासतौर से ध्यान देना जरूरी है."डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा, कंसलटेंट-इंफेक्शियस डिजीज, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
4. मलेरिया: यह सबसे प्रमुख संक्रामक रोगों में से है, खासतौर से दक्षिणपूर्वी भाग में. पिछले साल भारत में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आए यानी दक्षिणपूर्वी एशिया में 5.2 मिलियन मामलों मे से करीब 66% अकेले भारत में दर्ज किए गए.
जोखिमग्रस्त समूहों में कम उम्र के बच्चे और नवजात, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और उनके अजन्में शिशु शामिल हैं. मलेरिया के साथ और भी कई जटिलताएं जन्म लेती हैं, जिनमें सांस की समस्याएं, लो ब्लड शूगर, एनीमिया, आर्गेन फेल होना और सेरीब्रल मलेरिया प्रमुख हैं.
"हालांकि मलेरिया के मामले कम हो रहे हैं, तो भी 2022 में 0.8 मिलियन मामले दर्ज किए गए, जिनमें से आधे मामले खतरनाक फैल्सीपैरम स्ट्रेन से संबंधित थे. इस बीच, मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में कमी हुई है."डॉ. राजीव गुप्ता, डायरेक्टर– इंटरनल मेडिसिन, सी के बिड़ला अस्पताल®, दिल्ली
भारत सरकार ने जांच और निगरानी की नीतियों को लागू कर रखा है.
"वैक्सीन को मंजूरी मिलने और इसके उपलब्ध होने, अधिक जांच की सुविधाओं, शुरुआती डायग्नॉसिस और इलाज से संभव है कि भविष्य में इस रोग की गंभीरता को कम किया जा सकेगा."डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा, कंसलटेंट-इंफेक्शियस डिजीज, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम
5. डायरिया रोगः यह रोग 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खासतौर से खतरनाक होता है और बच्चों में असमय मौत का तीसरा प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 13% बच्चों की मौत होती है.
रोटावायरस ओर नॉरवॉक वायरस इस समस्या के प्रमुख कारण हैं और लंबे समय तक चलने वाले रोगों में कुपोषण की समस्या भी होती है.
इलाज के तौर पर ओआरएस, हाइड्रेशन प्रेक्टिस और बेहतर सेनिटेशन से मौतों को रोकने में मदद मिलती है. रोटोवायरस वैक्सीन भी उपलब्ध है.
6. निमोनिया: ये फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है और यह भी भारत में काफी फैलता है. वॉकिंग निमोनिया, जो कि निमोनिया का हल्का इंफेक्शन होता है, पिछले साल काफी चिंता का विषय बना रहा था. इसके अलावा भी सांसों के कई रोग हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं.
पैथोजन्स के आधार पर, तीन प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं – एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल. कई बार ऑक्सीजन थेरेपी और आईवी फ्लूड भी इलाज के तौर पर दिए जाते हैं.
नवजातों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को इस रोग का जोखिम अधिक रहता है.
7. एचआईवीः डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा बताती हैं कि यह रोग धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो भी देखने में आया है कि 15-49 आयुवर्ग में करीब 0.24% पुरुष और 0.20% वयस्क महिलाएं संक्रमित हैं और ज्यादातर मामले देश के नॉर्थईस्ट राज्यों में दर्ज किए गए हैं.
2019 में, लगभग 69,000 नए मामले दर्ज हुए, जो डेली इन्फेक्शन की ओर इशारा करते हैं.
इससे बचने के लिए सुरक्षित यौन व्यवहार, नशीले पदार्थों के सेवन के लिए सुइयों का प्रयोग और सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी उपाय हैं.
इन्हें रोकने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम क्या हैं?
संक्रामक रोगों में ट्यूबरक्लॉसिस (TB), टाइफायड, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, निमोनिया और एचआईवी देशभर के हेल्थकेयर सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. इस आर्टिकल में एक्सपर्ट्स ने लोगों को इससे बचने के कई उपाय बताए हैं.
एक्सपर्ट्स ने सरकार और समाज को इन बीमारियों को रोकने के लिए एक साथ मिल कर कदम उठाने की सलाह दी है.
"भारत में इन रोके जा सकने वाले रोगों से निपटने के लिए कई स्तर पर उपाय करने की जरूरत है. समय पर डायग्नॉसिस और जल्द इलाज शुरू करना बेहद महत्वपूर्ण है."डॉ. राजीव गुप्ता, डायरेक्टर– इंटरनल मेडिसिन, सी के बिड़ला अस्पताल®, दिल्ली
डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा फिट हिंदी से कहती हैं, "हेल्थ केयर में सुधार और रोगों से बचाव के उपायों को लागू करने के बावजूद काफी चुनौतियां बनी हुई हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि रोगों पर निगरानी रखने की जरूरत है. साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देते रहने की जरूरत है. इसके अलावा, आम जनता की सेहत के मामले में इन रोगों के खतरों को कम करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए".
इसके साथ ही एक्सपर्ट्स पब्लिक हेल्थ के लिए सालाना पर्याप्त बजट का प्रावधान करने की बात भी कहते हैं ताकि इन संक्रामक रोगों से कुशलतापूर्वक निपटा जा सके.